दुर्खीम का धर्म सिद्धान्त | Emile Durkheim Sociology of Religion
इमाइल दुर्खीम ( Emile Durkheim ) ने धर्म के समाजशास्त्र (Sociology of Religion ) में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने धर्म के उद्गम का विश्लेषण किया और मानव समाज में उसका कार्यभाग बताया। यही समाज में दुखींम के अनुसार धर्म के कार्य हैं।
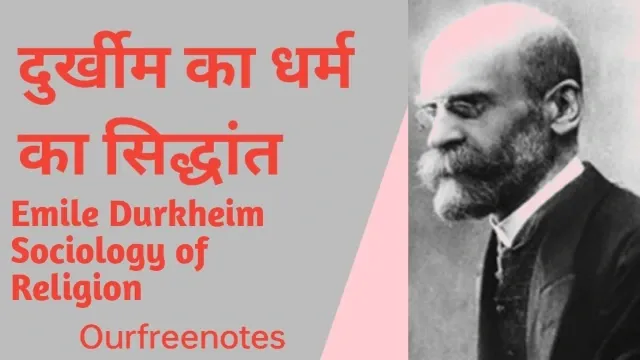 |
| Emile durkheim sociology of religion |
इस सम्बन्ध में इमाइल दुर्खीम की सन् 1912 में प्रकाशित धार्मिक जीवन के प्रारम्भिक रूप 'The Elementary Forms of Religious Life' शीर्षक पुस्तक उल्लेखनीय है । यह पुस्तक धर्म पर मौलिक रचना मानी जाती है। इस पुस्तक में दुर्खीम ने आस्ट्रेलिया के आदिवासी अरुन्टा (Arunta) जनजाति में टोटमवादी धर्म का विश्लेषण किया।
इस विश्लेषण के आधार पर उन्होंने धर्म के एक समाजशास्त्रीय सिद्धान्त का विकास किया है। उन्होंने धर्म के उद्गम के विषय में अन्य विद्वानों द्वारा दी गई व्याख्याओं का खण्डन किया । वे धर्म की व्याख्या पवित्र (sacred) वस्तुओं से सम्बन्धि विश्वासों और व्यवहारों की एक समन्वित व्याख्या के रूप में करते हैं। पवित्र वस्तुएँ वे हैं जो कि धार्मिक क्रियाओं के द्वारा अलग रखी गयी हैं ।
धर्म का अर्थ एवं परिभाषा(Meaning & Definition of Religion)
दुर्खीम ने अपनी पुस्तक में धर्म के स्वरूप और प्रकृति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। इस सम्बन्ध में उसने धर्म की प्रचलित अवधारणाओं की आलोचना की है। उसने स्वीकार किया है कि अलौकिक शक्ति में विश्वास को ही धर्म कहा जाता है। सामान्यतः इस अलौकिक शक्ति को ईश्वर के नाम से जाना जाता है। उसने धर्म को सामाजिक घटना माना है । इसीलिये इसकी विवेचना समाजशास्त्रीय आधार पर प्रस्तुत की है।
दुर्खीम ने धर्म की जो परिभाषा दी है वह निम्नलिखित है, “एक धर्म पवित्र वस्तुओं से सम्बन्धित विश्वासों एवं क्रियाओं की एक संकलित व्यवस्था है, अर्थात् जो पृथक् और निषिद्ध होती है - वे विश्वास और आचरण जिनको सभी मानते हैं, जो एक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित होते हैं और जिसे हम चर्च कहते हैं। दूसरा तत्व जिसका इस प्रकार हमारी विशेषता में स्थान है, प्रथम से कम आवश्यक नहीं हैं, यह दिखाने से कि धर्म का विचार चर्च से पृथकनीय नहीं है, यह इसे स्पष्ट कर देता है कि धर्म प्रमुख रूप से एक सामूहिक वस्तु होना चाहिये ।”
उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि दुर्खीम धर्म को सामाजिक वस्तु मानते हैं । इस सामाजिक वस्तु का निर्माण व्यक्ति के विश्वासों, क्रियाओं और व्यवहारों के योग से होता है। धर्म के आधार पर समूह के सभी सदस्य कुछ नैतिक आदर्शों के द्वारा परस्पर संगठित रहते हैं ।
पवित्र और अपवित्र की धारणा (Concept of Sacred and Profane)
दुखींम के धर्म का सिद्धान्त की व्याख्या में उनके द्वारा प्रतिपादित पवित्र और अपवित्र की धारणा भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने धर्म को सामाजिक घटना माना है। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने सामाजिक घटनाओं और वस्तुओं को दो भागों पवित्र और अपवित्र में विभाजित किया ।
धर्म उन वस्तुओं, घटनाओं तथा व्यवहारों से सम्बन्धित है जो पवित्र मानी जाती हैं। पवित्र वस्तुयें समाज या सामूहिक प्रतिनिधित्व की प्रतीक होती हैं और इसी कारण मनुष्य प्रायः अपने को तो उनसे नीचा मानते हैं और उन पर निर्भर करते हैं।
"पवित्र वस्तुयें वे हैं जिनकी निषेध संरक्षा करता है और पृथक करता है । अपवित्र वस्तुयें वे हैं जिन पर ये निषेध लागू हो ताकि पहली वस्तुओं से ये दूर रहे। पवित्र और अपवित्र दोनों एक-दूसरे के विपरीत हैं।"
सामाजिक घटना के इन दोनों भागों को कभी भी परस्पर नहीं मिलने देना चाहिये। इन दोनों को मिलाना पाप अथवा धार्मिक भ्रष्टाचार है। पवित्र वस्तुओं या विचारों की रक्षा जिन सामाजिक विश्वासों, विधि-विधानों, अनुष्ठानों और संस्कारों से होती है, उन्हें धर्म कहा जाता है। इस प्रकार धर्म की प सामाजिक विचारों एवं विश्वासों से होती है जिन्हें समाज पवित्र समझता है ।
धर्म की उत्पत्ति और उसकी सामाजिक व्याख्या (Origin of Religion and Its Social Explanation)
दुर्खीम से पूर्व यह विश्वास किया जाता था कि प्राकृतिक विपदाओं, तूफान, आँधी, भूकम्प तथा बाढ़ आदि के भय से धर्म की उत्पत्ति हुई ।
व्यक्ति अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है किन्तु ठीक ढंग से कार्य करने पर भी कभी-कभी उसको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। उस वक्त व्यक्ति यह सोच लेता है कि उसके प्रयासों को असफल बनाने वाली अदृश्य शक्ति अवश्य है।
व्यक्ति ने प्राकृतिक विपदाओं को भी अदृश्य शक्ति का ही रूप माना है। व्यक्ति ने इस सबके पीछे अदृश्य शक्ति का हाथ मानकर और अपने कार्यों में सफलता की कामना करके उस शक्ति को पूजा, भक्ति तथा उपासना आदि से प्रसन्न करने का प्रयास किया। इस प्रकार किसी अदृश्य शक्ति में विश्वास करने का नाम ही धर्म है। किन्तु दुर्खीम ने इन सभी विचारों की आलोचना की है। उनके मतानुसार ये सिद्धान्त धार्मिक घटनाओं के केवल एक पक्ष की व्याख्या करते हैं।
दुर्खीम ने प्राकृतिक शक्ति के स्थान पर सामाजिक शक्ति द्वारा धर्म की उत्पत्ति मानी है। जब व्यक्ति सामूहिक कार्यों में भाग लेते हैं तो उनमें साहस व उत्साह में वृद्धि होती है। समूह की शक्ति, व्यक्ति में विश्वास करती हैं। इसी विश्वास ने धर्म को जन्म दिया। समूह जिस कार्य की स्वीकृति देता है उसी को धर्म मान लिया जाता है। दूसरे शब्दों में दुर्खीम के अनुसार सामूहिक शक्ति ही अलौकिक शक्ति है जो धर्म का रूप धारण करती है।
दुर्खीम ने अपने धर्म की सामाजिक व्याख्या करते हुए बतलाया है कि - "धर्म का स्रोत स्वयं समाज है, धार्मिक अवधारणायें समाज की विशेषताओं के प्रतीक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, पवित्र या ईश्वर केवल मूर्तरूप समाज है और धर्म का सामाजिक कार्य सामाजिक एकता की उत्पत्ति, संरक्षण एवं स्थिरता है ।
दुर्खीम के मतानुसार मनुष्य की समाज और ईश्वर दोनों ही के प्रति समान मनोवृत्ति होती है। समाज अपने सदस्यों के मस्तिष्क में देवत्व की चेतना जागृत करने में अति है, क्योंकि इसका उन पर अधिकार होता है।
ईश्वर की ही भाँति समाज पर भी व्यक्ति एक निरन्तर निर्भरता की भावना रखता है। ईश्वर की ही भाँति समाज के पास नैतिक सत्ता होती है जिससे वह लोगों में निःस्वार्थ भक्ति और आत्म त्याग को जागृत कर सकता है। इसमें व्यक्ति को असाधारण शक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य है और वह सभी का मूल स्रोत है जो मानव व्यक्तित्व के लिये सर्वोत्तम तथा सर्वोच्च है।
स्वर्ग की सृष्टि विभूतिमान समाज है (The kingdom of heaven is a glorified society) । अतः जो धार्मिक मनुष्य किसी वाह्य नैतिक शक्ति पर विश्वास करता है वह किसी प्रकार के भ्रम में नहीं है क्योंकि इस प्रकार की शक्ति या सत्ता का अस्तित्व 'शक्ति और समाज' है।
धर्म की उत्पत्ति के प्राचीन सिद्धान्तों की आलोचना (Difference between Religion and Magic)
दुर्खीम ने धर्म की परिभाषा निर्धारित करने के पश्चात् धर्म के वैयक्तिक एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का खण्डन किया जिनमें प्रमुखतया टायलर (Tylor) का आत्मवाद (Anism) और मैक्समूलर का प्रकृतिवादी (Naturism) सिद्धान्त है।
(i) टायलर का आत्मवाद
टायलर के अनुसार आत्म की धारणा ही आदिम मनुष्यों से लेकर सभ्य मनुष्यों तक के धर्म के दर्शन का आधार है। यह आत्मवाद अथवा जीववाद (Animism) दो बड़े विश्वासों में बँटा हुआ है-
(अ) मनुष्य की आत्मा का अस्तित्व मृत्यु या शरीर के नष्ट होने के पश्चात् भी बना रहा है और
(ब) मनुष्य की आत्माओं के अतिरिक्त शक्तिशाली देवताओं की अन्य आत्मायें भी होती हैं।
टायलर के अनुसार आत्माओं में मनुष्य प्रतिदिन जीवन से सम्बन्धित दो प्रकार के अनुभवों के कारण विशेष रूप से उत्पन्न हुआ। ये दो अनुभव मृत्यु और स्वप्न थे ।
प्रथम अनुभव के आधार पर शरीर आत्मा (Body Soul) और दूसरी के आधार पर स्वतन्त्र आत्मा ( Free Soul) की धारणा उत्पन्न हुई। आत्मायें अमर तथा मनुष्य के नियन्त्रण से बाहर हैं। इसीलिये पूर्वजों की प्रथा प्रारम्भ हुई। यहीं से धर्म का श्रीगणेश हुआ।
दुर्खीम का कहना है कि टायलर ने आदिमवासी को एक दार्शनिक है समझकर ऐसी कल्पना कर ली है परन्तु वे अधिकांशतः बुद्धिहीन थे ।
(ii) मैक्समूलर का प्रकृतिवाद
इसके मतानुसार प्रकृति की विशालता को देखकर मनुष्य को असीम शक्ति का अनुभव हुआ है, यही धर्म है। प्रकृति के विभिन्न रूप देखकर व्यक्ति के मन में भय, आशा और आश्चर्य आदि होना स्वाभाविक था । इसके कारण से ही व्यक्ति के मन में श्रद्धा और भय की भावना उत्पन्न हो गयी। इसी भावना से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ।
दुर्खीम इस प्रकृतिवादी, प्रकृतिपूजक को भी ठीक नहीं मानता। धर्म का रूप प्रकृतिपूजा करना ही नहीं है, धर्म मानव जीवन को प्रभावित करने वाली एक अद्वितीय शक्ति भी है ।
दुर्खीम ने इन सभी सिद्धान्तों के प्रति मुख्य रूप से तीन आपत्तियाँ उठाई हैं-
- ये सिद्धान्त धार्मिक घटनाओं के सम्पूर्ण निकार्य (Whole body of religious phenomena) के केवल एक ही भाग पर विचार करते हैं।
- ये पवित्र एवं अपवित्र की विषमता पर कोई प्रकाश नहीं डालते जो धर्म की प्रमुख विशेषता है।
- ये धर्म की व्याख्या एक ऐसे मायाजाल (Illusion) के रूप में करते हैं, जिसका वास्तविक जगत में कोई सम्बन्ध नहीं है।
धर्म का उद्गम (Origin of Religion)
धर्म के उद्गम की व्याख्या के विषय में दुखीम ने टायलर (Tylor ) और स्पेन्सर (Spencer) के जीववाद (Animism) और मैक्स मूलर (Max Muller) के प्रकृतिवाद (Naturism) का खण्डन किया है। दुखींम का कहना है कि ये दोनों ही सिद्धान्त पवित्र और अपवित्र में अन्तर की व्याख्या नहीं करते। धर्म कोई रहस्य नहीं है। वह किसी परात्पर (transcendental) ईश्वर में विश्वास नहीं है, वह कोई विभ्रम (illusion ) नहीं है । सम्पूर्ण इतिहास में मनुष्यों ने कभी भी समष्टिगत सामाजिक सवस्तु के अलावा किसी अन्य संत की उपासना नहीं की और केवल इसे ही आस्था से विभूषित किया और ईश्वर कहा ।टोटम के प्रसंग में धर्म के उद्गम की व्याख्या करते हुए उन्होंने आस्ट्रेलियाई जनजातियों में इसका विश्लेषण किया। उन्होंने लिखा है, "टोटमवाद एक धर्म है, कुछ पशुओं अथवा कुछ मनुष्यों अथवा कुछ प्रतिमाओं का नहीं, बल्कि एक अनाम और अवैयक्तिक शक्ति को जो कि इन प्राणियों में पायी जाती है, किन्तु वह उनमें से किसी से भी तादात्मय नहीं की जाती है। कोई भी उसे पूर्णतया नहीं रखता और सभी उसमें भाग लेते हैं। वह विशिष्ट विषयों में इतनी स्वतन्त्र है कि वह उनके पूर्व होती है और उनके लिये पर्याप्त होती है। व्यक्ति मरते हैं, पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं और उनका स्थान दूसरी पीढ़ियाँ ले लेती हैं परन्तु यह शक्ति सुदैव उपस्थित, जीवित और अपने प्रति सच्ची रहती है। वह वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा देती है जैसी कि उसने गुजरे हुए कल को दी थी और जैसी कि वह आने वाले कल को देगी।”
धर्म शब्द को अत्यन्त व्यापक अर्थ में लेने पर यह कहा जा सकता है कि वह ईश्वर है जिसकी प्रत्येक टोटमवादी सम्प्रदाय में पूजा की जाती है; परन्तु वह एक निर्वैयक्तिक ईश्वर, अनाम, बिना किसी इतिहास के, जगत में उपस्थित और असंख्य वस्तुओं में फैला हुआ है । इस विश्लेषण के आधार पर दुर्खीम धर्म की परिभाषा करते हुए उसे उन वस्तुओं के विश्वासों और विधि विधानों की एक परस्पर निर्भर व्यवस्था मानते हैं जो कि पवित्र हैं और जो कि विश्वासों और विधि विधानों के द्वारा उन सबको एक सूत्र में बाँधती हैं और अनुयायियों को मिलाकर एक नैतिक समुदाय बनाती है जो कि चर्च कहलाता है।
धर्म के सच्चे विज्ञान की अपने सिद्धान्त से तुलना करते हुए वे जीववाद और प्रकृतिवाद को अर्धवैज्ञानिक सिद्धान्त कहते हैं। उन्होंने यह दिखलाया है कि धर्म को विभ्रम नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसे मानव इतिहास में सदैव एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और सभी युगों में मनुष्यों ने उससे प्रेरणा प्राप्त की है। यह सर्वविदित है कि कानून नैतिकता और स्वयं वैज्ञानिक विचार भी धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं, लम्बे काल तक वे धर्म का अंश थे और उनमें सदैव धार्मिक भावना का राज्य रहा है। इस प्रकार की मानव चेतना का निर्माण करने वाली व्यापक शक्ति को विभ्रम कहा जा सकता है। प्रत्येक विज्ञान प्राकृतिक जगत से सम्बन्धित होता है । अस्तु, धर्मों के विज्ञान के लिये यह सिद्धान्त होना ही चाहिये कि धर्म प्रकृति में जो कुछ नहीं है उसके विषय में कुछ नहीं कहता ।
दुर्खीम की धर्म की अवधारणा की आलोचना ( Criticism of Durkheim's Concept of Religion )
दुर्खीम की धर्म की अवधारणा की आलोचना करते हुए रेमंड आरन ने कहा है, “मुझे सन्देह है कि यह धर्म की किसी भी परिष्कृत व्याख्या के विषय में कहा जा सकता है; किसी धर्म का समाजशास्त्र भी मामले में, एक विशुद्ध रूप से मानवीय अवधारणा में, नैतिक मूल्य मानवता की सृष्टि हैं। मनुष्य पशु जाति का एक प्रकार है जो कि क्रमशः मानवता पर आरोहण करता है । यह भावना कि कोई ऐसी वस्तु है जिसका आन्तरिक मूल्य है, धर्म के अर्थ को ही बिगाड़ देना है अथवा मानव नैतिकता के अर्थ को गड़बड़ा देना है।" दुर्खीम ने यह माना है कि समाज और दिव्य तत्व की तुलना की जा सकती है और उन्हें प्रत्यक्ष की वस्तुयें माना जा सकता हैंइस अवधारणा में दोष यह है कि ईश्वर के नाम पर राष्ट्रीय एकता को बनाये रखते हुए राष्ट्र पूजा की ओर ले जा सकता है जिसका परिणाम नाजीवाद और फासीवाद के रूप में क्रमश: जर्मनी और इटली में तानाशाहियों के विकास में देखा जा सकता है। वास्तव में दुर्खीम विज्ञान और धर्म के अन्तर को भूल जाते हैं। इन दोनों में बाह्य समानतायें होने के बावजूद विज्ञान का सम्बन्ध तथ्यों से है जबकि धर्म का सम्बन्ध तथ्यों से न होकर मूल्यों से होता है । फिर भी, इसमें सन्देह नहीं कि एमाइल दुर्खीम ने आधुनिक मानव चेतना के अनुरूप धर्म की एक अधिक विवेकयुक्त अवधारणा उपस्थित करने का प्रयास किया है।
धर्म के प्रमुख कार्य ( Functions of Religion )
दुर्खीम के अनुसार धर्म के निम्नलिखित कार्य हैं-
- धर्म मानव जीवन को दो पक्षों- पवित्र एवं अपवित्र में विभक्त करता है ।
- धर्म अपने सदस्यों को इन दोनों पक्षों को अलग रखने की शिक्षा देता है क्योंकि पवित्र जीवन से दूर हो जाना धार्मिक भ्रष्टाचार है।
- धर्म लोगों को यह शिक्षा देता है कि सामान्य अपवित्र क्रिया वाले स्थान से धर्म का स्थान अलग होना चाहिये और दैनिक उपयोग के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग नहीं होना चाहिये ।
- धर्म अपवित्र कार्यों के करने पर धार्मिक शुद्धि (Religious Purification) करने का आदेश देता है ।
- धर्म समाज को संगठित एवं नियन्त्रित करता है।
दुर्खीम के धार्मिक विचारों की आलोचना (Criticism of Religious Views of Durkheim)
- दुर्खीम ने अरूण्टा जनजाति को सबसे आदिम (Primitive) जनजाति माना है परन्तु कुछ विद्वान उसकी इस बात से सहमत नहीं हैं ।
- दुर्खीम का यह कथन भी गलत है कि टोटमवाद धर्म का सर्व प्रमुख तथा सर्वप्रथम आधार है।
- दुर्खीम की यह बात भी टोक नहीं मालूम होती है कि हमारा ईश्वर और समाज के प्रति दृष्टिकोण समान है, विशेष रूप से उस समय तो यह ठीक नहीं माना जा सकता है, जब हम समाज और संस्कृति में अन्तर करते हैं। यदि दोनों में समानता सिद्ध भी कर जाए तो यह सिद्ध नहीं हो सकता है कि ईश्वर और समाज एक ही है।
- दुर्खीम का यह सिद्धान्त धार्मिक व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाता है।
- धार्मिक व्यक्ति कभी भी समाज को ईश्वर नहीं मानते और न ही उसकी पूजा कर सकते हैं।
- दुर्खीम का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता कि अनुष्ठानों एवं उत्सवों में सामाजिक कारक धार्मिक भावना को स्पष्ट एवं प्रगाढ़ कर देते हैं ।
- धर्म की उन्नति में सामाजिक कारक ही एकमात्र कारक नहीं है ।
